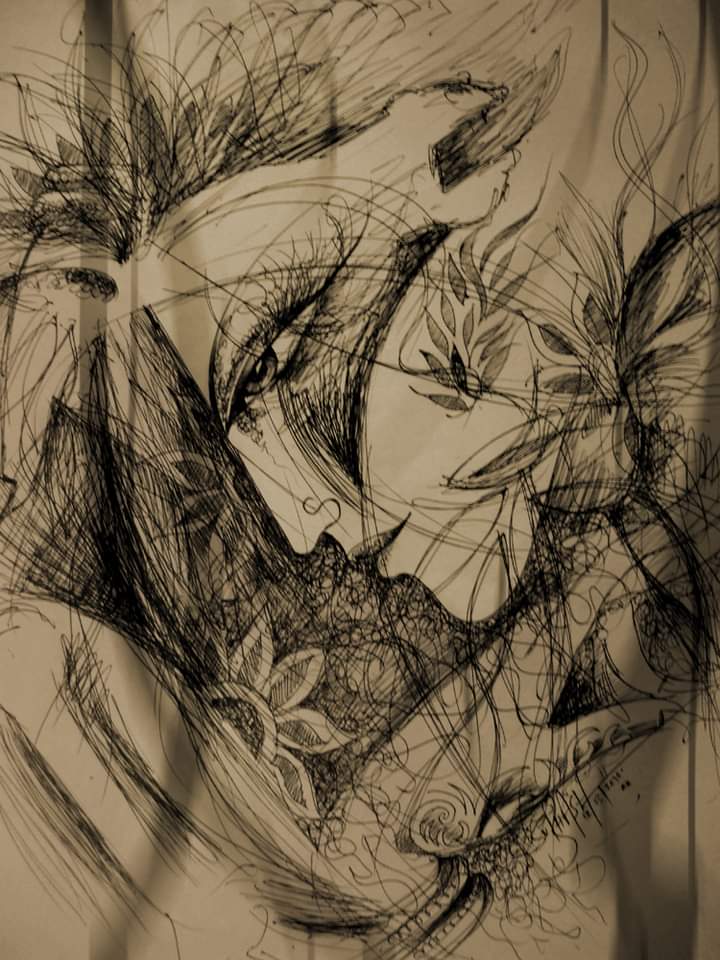प्रस्तुति: अरविंद कुमार
साभार-स्त्री दर्पण
आज कृष्णा सोबती का जन्म दिन है।आपके लिए उनकी बहुचर्चित कृति “ऐ लड़की” की भूमिका पेश की जा रही है।1992 में वर्तमान साहित्य के कहांनी विशेषांक में यह कहांनी छपी थी जिसका संपादन रवींद्र कालिया जी ने किया था।उस समय यह हिंदी की सबसे लंबी कहांनी थी।उसके बाद तो हिंदी में लंबी कहानियां लिखने का चलन ही शुरू हो गया।राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक कृष्णा सोबती रचना का गर्भ गृह से साभार यह भूमिका हम दे रहे है।इसका सम्पादन हिंदी कवि चेतन क्रांति ने किया है।
**********
ऐ लड़की!
अम्मू विधिवत् इस दुनिया से लौट गई थीं। सगे-सम्बन्धी अपने-अपने घर- परिवारों को जा चुके थे।
सुबह जगी तो घर के कोनों, कमरों में अम्मू दीखने लगीं। मैं अपने लिए सजग और सतर्क हो उठी।
बस इतना ही दूर हो जाओ इस ठंडे तापमान से।
फ़ोन बजा ।
मित्र प्रकाशक- शीला सन्धू ।
हमारा प्रोग्राम बदला है। हम इस महीने बाहर नहीं जा रहे। पहलगाँव में बुकिंग है। आप चाहें तो जा सकती हैं। मेरी ओर से थी तत्काल सहमति!
श्रीनगर से पहलगाँव पहुँची तो पानी बरस रहा था। लगा मेरे लिए बरसा है।
टूरिस्ट ऑफ़िस से रिज़र्वेशन स्लिप दिखा कॉटेज का नम्बर लिया और चौकीदार साहिब के साथ ऊपर पहुँच गई। कॉटेज सबसे ऊपर थी। एकान्त । सामने पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ थी।
नीचे लिद्दर का शोर था। दोनों बाथरूम के गीजर ठीक थे। किचन में गैस और बर्तन मौजूद थे।
-सुबह की चाय तो आप देंगे न! –नहीं साहिब। यह तो आपको खुद ही करना होगा।चाय चीनी दूध लगाकर रख दूंगा आज। सुबह की चाय बनाने का कोई उद्यम नहीं था। बाकायदा पाँच दिनदस बजे तक सोती रही।
फिर कुछ हुआ कि चौकीदार साहिब सुबह की चाय देने लगे। एक दिन नाश्ते के बाद देर तक बरामदे में बैठी रही। ढलानों के सब्जे
भी चलने, दौड़ने को न उकसा सके। चौकीदार साहिब श्रीनगर जा रहे थे। दोपहर दो की बस से। पूछा- कुछ मँगवाना तो नहीं वहाँ से!
— नहीं! शुक्रिया।
लंच के बाद फिर अन्दर जा लेटी।
नींद में देखा, कॉटेज के आसपास सब्ज़ ढलानों पर लोग बैठे हैं-कुछ ऐसे कि कोई जश्न, जलसा हो! मेरे बरामदे में से आ रही है। आवाज़ सरोद की। उठी। खड़ी हो गई। जाना होगा मुझे बस स्टॉप पर। अगर चौकीदार साहिब
न मिले तो मुझे श्रीनगर जाना होगा। काग़ज़ ख़रीदने के लिए!
चौकीदार साहिब बस के सामने खड़े थे—
क्यों साहिब?
लिफ़ाफ़ा आगे किया। आपको मेरे लिए लिखने के काग़ज़ लाने होंगे।
साइज और ब्रांड लिख दिया है।
-सुबह पूछा था न आपसे। तब क्यों न कह दिया!
-तब और बात थी।
इत्मीनान से घूमते-घामते हल्के मन से पहलगाँव क्लब पहुँच गई। चाय । रंग-बिरंगे ढेरों फूल थे। लिद्दर का शोर था । गोल-गोल पत्थरों पर पैर ड़ाता छलकता पानी था। गोरे-चिट्टे ख़ूबसूरत कश्मीरी बच्चे थे।
लौटते हुए गुरुद्वारे के सामने से निकली तो अन्दर जा माथा टेका। लगा अम्मू वहाँ बैठी पाठ सुन रही हैं।
बाजार से कश्मीरी तश्तरी खरीदी और साथ ली लाल सुर्ख चेरी।
रात मेज़ पर बैठी तो अम्मू चुपचाप कमरे में आ विराजमान हो गई। कलम उठाई तो आवाज आई- ऐ लड़की!
मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं कि ‘ऐ लड़की’ को कहानी कहा जाए। संवादपरक होते हुए भी इस वृत्तान्त में कहीं कुछ ऐसा है जो इसे लम्बी कहानी का रूप देता है। ग़लत यह भी नहीं कि इसे यदि नाटक में रचा जाता तो शायद यह कहीं ज्यादा उपयुक्त होता। संवाद इस साधारण और असाधारण मुखड़ेवाली स्थिति की माँग थी।
लेखक की सीमाएँ इसे नाटक की तरतीब न दे सकीं, यह स्वयं मेरे लिए चिन्ता का विषय रहा। किसी भी गद्य लेखक की यह महत्त्वाकांक्षा होती है कि वह अपनी रचनात्मक अवधि में एक नाटक तो प्रस्तुत कर सके। ऐसा नहीं हो पाया, इसके लिए अपनी असमर्थता स्वीकार करनी होगी।
जिन्दगी को जीने का यह जो रोजमर्रा का अभ्यास है इसे हम निरन्तरता नहीं कहते। बीमारी की उपस्थिति जो कि ‘टर्मिनल’ हो अपने में एक नाटकीय अंश सँजोए रहती है जो मानवीय तन और मन का अन्तिम अध्याय है, और जब यह मौजूद हो तो कुछ नाटकीय स्थितियाँ ऐसी घटती हैं जो आमतौर पर रोजमर्रा की जिन्दगी के बाहर होती हैं। जब मैंने इसे लिखना चाहा तो लगा कि क्योंकि वहाँ नाटक था, ऐसा नाटक जो नाटक नहीं था और था भी, तो क्यों न इसे नाटक में ही लिखूं। पर बाद में यह सोचकर कि मुझमें शायद इस बात की क्षमता नहीं है इसे नाटक में समेटने की, मैंने इसे कहानी के रूप में उतार लिया। यह मानकर कि मैं अपनी चीज़ को अपनी सीमाओं के कारण क्यों बिगाहूँ ।
‘ऐ लड़की’ के बीज मंत्र की ओर लौटें तो कहना होगा कि जिन शब्दों ने इस कहानी की पहली आहट मुझे दी थी वे तो कहानी के बाहर ही खड़े
रह गए। शब्द ‘चिराग जलता रहेगा-चिराग जलता रहेगा-विरा रहेगा।’ लेखक शब्दों से सरसरी तौर पर काम नहीं लेता। वह और संवेदनाओं को एक-साथ चाहता है। शब्द ऐसे जो भारी न न सतही, न मूक, मुख, नवनी, न हवा में लहराते भाषा है, जिसे लेखक अपने अन्तर में महसूसता है और अपने बाहर को सोखता है, अपने में जब करता है, गोचर और अगोचर को शब्दों में साधता है। निपुणता न लेखक की और न शिल्प के कौशल की ही।
जाती हुई, विदा देती और विदा लेती स्त्री पुरानी है, पर उसमें की आहट नई है। उसके नए की आहट है। स्त्री न मात्र बेटी है, न पत्नी, न सिर्फ मौ वह इन सब में गुथा एक व्यक्तित्व है जो उसके गुण और उपयोगिता से, उसके वैयक्तिक मूल्यों से परे उसके निज के आत्मधर्म से गुँथा है और उसकी काया के नीचे छिपा है। अपनी पूरी उपस्थिति के साथ। यही स्त्री का भविष्य है। सम्बन्धों की सघनता के पार अब यही उसका वक्तव्य है। जीवन और के प्रतिपक्ष में, यही उसकी नई चेतना की खोज है: बदलो, अपने देह- के पार देखो, नई चेतना को स्वीकारी। अपने संस्कार की चेतना तुम्हें स्वयं होना है। स्त्री के जैविक स्वभाव को मात्र माँ का अक्स समझना, उसे अ करके देखना है। उसके व्यक्तित्व की पहचान उसकी आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ी है। गद्य की स्पष्टता और उसके वैचारिक और सामाजिक खरेपन ने मुझे लगातार अपनी ओर खींचा है। अपनी कशिश विशेष से उकेरा भी है। एक ही मुखड़े और तेवर वाली भाषा में सोचना और लिखना मुझे उबाऊ लगता है। रचना के रचनात्मक केन्द्र में लेखक के संवेदन के साथ-साथ भाषा ही उसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर रचना को व्यापक बनाती है। अपने को अपनी बँधी-बँधाई चौखट से परे सरकाकर पात्रों के अनुरूप भाषा, मुहावरे और संवाद को ढालना मुझे मात्र प्रयोग नहीं, लेखकीय सामर्थ्य का अहसास भी करवाता है, नई भाषा गढ़ने का साहस भी देता है।