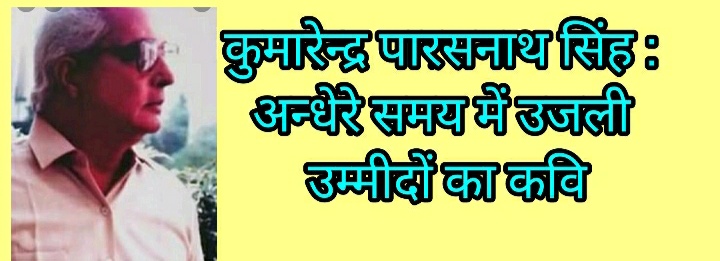लेखक परिचय –
लेखक परिचय –
नाम – उमाशंकर सिंह परमार
काम- पढना , लिखना ,समाज सेवा , किसान आन्दोलन से जुडाव , जनवादी लेखक संघ उत्तर प्रदेश का राज्य उप सचिव
विधा– आलोचना , कभी कभार कविता
पुस्तक – प्रतिपक्ष का पक्ष ( आलोचना) , सुधीर सक्सेना – प्रतिरोध का वैश्विक स्थापत्य ( आलोचना) ,समय के बीजशब्द ( आलोचना ) पाठक का रोजनामचा
( आलोचना ) कविता पथ ( आलोचना ) सहमति के पक्ष में ( प्रकाशकाधीन आलोचना ) – हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं जैसे चिंतन दिशा , व्यंजना , कृति ओर , हिमतरु , नयापथ , हंस , प्रयाग पथ , मंतव्य सप्तपर्णी , दुनिया इन दिनों , स्वाधीनता , वर्तमान साहित्य , जनपथ , लहक , प्राची , लमही , सुखनवर , जन्संदेश टाइम्स , लोकलहर , रस्साकसी , अनहद , माटी , वसुधा , यात्रा , लोकोदय , बाखली , प्रसंग बिहान ,मंतव्य छत्तीसगढ़ मित्र , बुन्देलखंड कनेक्ट आदि में आलेखों का प्रकाशन |
महत्वपूर्ण ब्लॉगों में प्रकाशन , लोकविमर्श ब्लॉग एवं आलोचना पत्रिका का लोकविमर्श का संपादन ,
पता –द्वारा गऊलाल डाकिया , प्रधान डाकघर अतर्रा रोड बबेरू , जनपद बाँदा 210121
इमेल – umashankaersinghparmar@gmail.com
फोन – 09838610776
कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह – अन्धेरे समय में उजली उम्मीदों का कवि
रचनाकार:- उमाशंकर सिंह परमार
जनवादी लोकधर्मी गीतकार कवि कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह के लिखे हुए का बहुत सा हिस्सा आज नये लेखकों और कवियों के पास उपलब्ध नही हैं । मगर जो भी उपलब्ध है इस कवि की लोकचेतना और जमीनी सौन्दर्यबोध की वैचारिक विनिर्मिति को समझने के लिए पर्याप्त है ।कविता में विचारधारा की वास्तविक अभिव्यक्तियाँ पूँजीवादी दौर में किस तरह उपेक्षित की जाती हैं कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह इसके उदाहरण हैं ।पारसनाथ सिंह किसी भी बडे कवि के समक्ष कमजोर नही हैं और अकादमिक संस्थानों व पीठों द्वारा विनिर्मित देवमूर्तियों से उन्नीस नही है बीस ठहरते हैं किसी भी नजरिए से देखा जाए मुद्दा प्रतिबद्धता का हो या जीवन में शुचिता ( छल छद्म)का कुमारेन्द्र सबसे कोसों आगे हैं । बस कमजोर रहे है तो सत्ता और कारपोरेट द्वारा प्रायोजित परिचर्चाओं का मामलों और अकादमिक आलोचकों की मिजाजपुर्सी में शायद यही कारण है मुक्तिबोध , केदारनाथ सिंह , अशोक बाजपेयी , नामवर सिंह के साहित्येतर कर्मों के कारण मजबूरी में परिचर्चा करता हुआ सरकार का करोडों रूपया बर्बाद करने वाला हिन्दी का कृतघ्न समुदाय आज कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह के अवदान को विस्मृत कर चुका है । पारस नाथ सिंह का जन्म चार जनवरी उन्नीस सौ अट्ठाईस को बिहार राज्य के बक्सर जिले के अति पिछडे गाँव चौगाई मे हुआ था काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से एम ए करने के बाद यहीं किसी कालेज मे मास्टरी की फिर लम्बे समय तक कोलकाता मे पढाते रहे बसे लम्बे समय तक पटना के अनुग्रह नारायण सिंह कालेज में पढाया 1969 से 1990 तक यहाँ व्यख्याता पद पर रहे ।

चौबीस जून 1992 में इनका देहान्त हुआ देहान्त के बाद बहुत सी पत्रिकाओं ने इन पर विशेषांक निकाला और चर्चा की यह हिन्दी में अक्सर होता आया है । बबुरीवन कविता संग्रह इनके जीवनकाल मे प्रकाशित हो चुका था पत्थरों के गीत और बोलो मोहन गाँजू इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए । काव्यभाषा का वामपक्ष इनकी सुप्रसिद्ध आलोचना कृति रही जिसे अपनी स्थापनाओं के कारण आज भी याद किया जाता है ।
कुमारेन्द्र बीसवीं सदी के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं वामपंथी चिन्तक थे और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित एक्टिविस्ट थे ।लेखन और जीवन के साम्यता का इनके जैसा उदाहरण शायद ही हिन्दी मे दूसरा प्राप्त हो।इतिहास का संवाद उनकी पहली काव्य कृति है जिसमे उन्नीस सौ पैंसठ से लेकर सतत्तर तक की उन्नीस गम्भीर और वैचारिक आयतन से विस्तृत कविताएँ संकलित हैं । यह वह दौर था जब रूपवादी काव्य का बोलबाला था हिन्दी हलकों मे कविता की वापसी का शोरगुल बढता जा रहा था । साठ के दशक के मोहभंग का परिपक्व और बचा खुचा स्वर पारसनाथ सिंह में जिन्दा था उन्होने कविता की वापसी का विरोध करते हुए इसकी रूपवादी मनोवृत्ति को जगजाहिर कर दिया । जनवादी लोकधर्मी कविता की अलख को जगाए रखा । 1965 से 1970 तक की पीढी मे बडे बडे नाम थे जिन्होने ने केदार त्रिलोचन नागार्जुन की परम्परा को घोर संकट के समय भी बचाए रखा इन कवियों में कुमारेन्द्र पारस नाथ सिंह , विजेन्द्र , वेणुगोपाल , विष्णुचन्द शर्मा , महेन्द्र भटनागर , मलय , भगवत रावत , जैसे कवि थे ।
इस पीढी मे कुमारेन्द्र दूर से ही पहचाने जा सकते हैं । कारण इसलिए कि काव्यभाषा और काव्यरूप दोनो स्तरों से वह जनवादी रहे । काव्यरूपों में उनकी पसंदीदा शैली गीत की रही है ।गीतों की अनुकृति नवगीत जैसे आन्दोलन की नही बल्कि लोकछन्दों और लोकरूपों की है । और भाषा अपने समय की वैज्ञानिक भाषा थी । जिसमे नागार्जुन जैसी प्रतिबद्धता , केदार जैसी जनपदीयता और त्रिलोचन जैसी दूध मे मिले हुए पानी समान विचारधारा रही है । लय विन्यास और स्वर की वैचारिक परिपक्वता को देखकर ही नामवर सिंह ने कुमारेन्द्र की तुलना “निराला” से की थी ।

कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह की संवेदना अत्यन्त संघन एवं आत्मीय है वह विस्तारण की बजाय संक्षिप्त तफसीलों पर अधिक मन रमाते हैं । अपनी उम्मीदों से सरोबोर कवि का सौन्दर्यबोध जीवन के प्रति बडा ही भावुक होता है वह प्रकृति की मानवीय सत्ता और उसकी वैविध्यपूर्ण छवियों मे अपने आप की लय को अन्तर्लय कर देता है । वैयक्तिक लय को समूची प्रकृति मे लय कर देना और भाषा की व्यंजना को आवेग को सौंप देना अपने आप को निर्वैयक्तिक कर उम्मीदों से जीवन निचोडना वामपंथी सौन्दर्यबोध का अलहदापन है जो कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह की कविता को आज भी ताजा रखता है और कविता की इस भारीभरकम भीड मे सबसे अलहदा रखता है उनकी एक कविता है “वह नदी मे नहा रही है” इस कविता का बिम्बविधान कवि के इस सौन्दर्यबोध का परिचय देती है यह जीवन के भीतर का जीवन्त बोध है और उम्मीदों की अतिसघन प्राथमिकताओं के बीच अपनत्व के अहसास का बिम्ब है देखिए यह गीत “ वह नदी में नहा रही है / नदी धूप में /और धूप उसके जवान अंगों की मुस्कान मे / चमक रही है।/ मेरे सामने / एक परिचित खुश-बू / कविता की भरी देह में खड़ी है / धरती यहां बिल्कुल अलक्षित है / अंतरिक्ष की सुगबुगाहट में / उसकी आहट सुनी जा सकती है। / आसमान का नीला विस्तार / और आत्मीय हो गया है।
यहाँ कविता आसमान और उसका विस्तार कविता का अन्त होते होते कवि की उम्मीदों के साथ खुद को जोड देता है । यह है कवि की कविता का स्रोत । जब कवि अपनी कविता का स्रोत अनन्त जीवन के विस्तारित क्षणों की लाजवाब उम्मीदों मे अन्वेषित करता है तो वह अपने आप को उस रीति से जोड रहा होता है जहाँ से कविता का उत्स होता है ।बाल्मीकि की पहली कविता जीवन के बिम्ब से निकली थी और कुमारेन्द्र भी कविता का स्रोत जीवन के सचेष्ट राग मे खोज रहे हैं । जीवन प्रति यही आसक्ति कुमारेन्द्र को अपने समय से बहुत आगे खडा कर देती है । जीवन मे दो पक्ष होते हैं एक पक्ष अभावों से जूझ रही अस्मिताओं का और दूसरा पक्ष सम्पत्ति और अधिकारों मे खेल रही केन्द्रीय अस्मिताओं का । पारसनाथ का पक्ष अभाव का पक्ष है यह उनकी वैचारिक अवस्थिति है । जब हिन्दी मे दलित आन्दोलन की सुगबुगाहट भी नही थी उस समय दलित अस्मिताओँ पर बडी यथार्थवादी कविताओं को लिखा । दिल्ली के अकादमिक आलोचक लोकधर्मी कविताओं पर यह आरोप लगाते हैं कि यहाँ आधुनिक अस्मिताओं की उपेक्षा है और लोक का भरा पूरा सामन्ती सौन्दर्य ही लोकधर्मिता है उन्हे कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह की कविता पढनी चाहिए विशेषकर भंगी कालोनी , और हरिजन टोली कविताओं को पढना चाहिए यह कविताएं नागार्जुन जैसी राजनीति तो नही करती पर आक्रोश और उम्मीद मे किसी भी समकालीन कवि से बेहतर कविताएं हैं।
सर्वहारा प्रेम का अदभुद और वास्तविक बिम्ब जो पाठक के ह्दय को भी झकझोर देता है कुमारेन्द्र की भंगीकालोनी कविता मे है । “बाबू जरा ई तो बताओ / ई भंगी और अछूत का होता है / जिसकी जेब मे पैसा / और हाथ मे अधिकार होता है / वह आदमी फिर दूसरा कैसे हो जाता है” यहाँ दलित और सवर्ण का मामला जातिगत प्रतिमानों और आम्बेडकरवादी शुष्कता मे नही आया है जो सामन्ती और ब्राम्हणवादी उपादानों के सहारे ही विमर्श को आगे बढा रहे हैं इस कविता मे वर्गीय दृष्टि है अभाव और पीडा का कारण अधिकार और पूँजी का असमान अधिपत्य है । यही है वैज्ञानिक नजरिया । इसी तरह हरिजन टोली कविता को देखिए “हरिजन टोली में शाम बिना कहे हो जाती है। / पूरनमासी हो या अमावस / रात के व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। / और जब दिन के साथ चलने के लिए / हाथ-पैर मुश्किल से अभी सीधे भी नहीं हुए रहते, / सुबह हो जाती है।“
यह कविता भी शोषित समाज की दलितवादी कविता है इसे कोरी संवेदनाओं से लैस राजनीति का मामला नही कहा जा सकता है जैसा कि आज की कविताओं को कहा जा रहा है क्योंकी यहाँ जीवन के मूलभूत अनुभवों को जिसके अभाव में जीवन पत्थर जैसा हो जाता है उस सवाल को उठाया गया है । पूँजी व्यक्ति का विस्थापन करती है और पूँजीवाद अलगाव की सैद्धांतिकी पर काम करता है । अलगाव करूणा , मोह , ममता व सौन्दर्यबोध से व्यक्ति को पृथक कर देता है । यहाँ दलितों की बस्ती मे इसी आलगाव की अभिव्यंजना की गयी है । विचारधारा के सहारे समस्त असंगतियों को विवेचित करना और समस्याओं को इतिहासबोध की सीमा मे दाखिल कर मानवीय संवेदना का सृजन करना पारसनाथ सिंह को अपने समय का बडा कवि बना देता है यह विशेषता उस युग मे केवल मलय की कविताओं मे पायी जाती है ।
कुमारेन्द्र लोकधर्मी कवि हैं लोकबिम्ब और लोकजीवन की चलती फिरती दृष्यावलियाँ उनकी कविता में बहुतायत हैं।
इन दृष्यावलियों की सबसे बडी विशेषता है कि वह लोकभाषा में है और लोक की शब्दावली में ही मूर्तमान होते हैं ।लोकधर्मी कविता में बिम्बों का महत्व बहुत पहले से रहा है रूपवादी कवि अधिकतर महानगरीय जीवन जीते थे इसलिए उनकी कविता मे सर्वहारा जीवन की कठिनाईयाँ नही दिखाई देती हैं यदि ऐसे बिम्ब आते भी हैं तो अनदेखे और अनजाने होने के कारण असंगत और नकली प्रतीत होते हैं जैसे केदारनाथ सिंह , मंगलेश बडराल , आदि में । लोकधर्मी कवि अधिकतर अपने लोक मे रहते हैं वह स्मृतिपरक बिम्बों की बजाय वास्तविक और अनुभूत बिम्बों का अधिक प्रयोग करते हैं ।विजेन्द्र का कहना है कि ” बिम्ब से दूर जाने का अर्थ है हम जीवन समाज और प्रकृति से कट रहे हैं” बिम्ब वास्तविकता को मूर्त करते हैं ।
व्यक्ति के अनुभव को प्रमाणित करते हैं वास्तविक बिम्ब का सृजन वही कर सकता है जो जीवन और जगत के क्रियाशील पक्ष से जुडा हो जैसे कि कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह के बिम्ब क्रियाशील जगत की मूर्तमान सत्ता है । पारसनाथ सिंह समस्याओं का गाना नही गाते बल्कि बिम्ब देकर पाठक को समझने और समझाने का दायित्व सौंप देते हैं देखिए हरिजन टोली कविता का एक बिम्ब जो जीवन को उलझाता नही है जबरिया हस्तक्षेप नही करता है साथ चलने वाली विचारधारा के प्रभाव से वह खुद की प्रमाणिकता को साबित कर देता है “कहीं रमिया झाड़ू-झंखा लेकर निकलती है / तो कहीं गोबिंदी गाली बकती है। / उसे किसी से हँसी-मजाक अच्छा नहीं लगता / और वह महतो की बात पर मिरच की तरह परपरा उठती है।/ वैसे, कई और भी जवान चमारिनें हैं, / हलखोरिनें और दुसाधिनें हैं, / पर गोबिंदी की बात कुछ और है / वह महुवा बीनना ही नहीं, / महुवा का रस लेना भी जानती है।“
जीवन से जुडे ऐसे बिम्बों का पारसनाथ सिंह की कविता मे बहुतायत प्रयोग हुआ है यहाँ जीवन की संगति है और जीवन की उम्मीद का राग भी है । राग और जीवन का पारस्परिक आमेलन कवि की सृजन विधायनी क्षमता का लोहा मानने को मजबूर करता है यहाँ महानगरीय जीवन की अपेक्षा कस्बाई और ग्रामीण बिम्बों व अन्तर्विरोधों का विस्तारित फलक है । सर्वहारा की घुटती साँसों का एक एक रेखांकन है । यहाँ खेत , जंगल , किसान , मजदूर , स्त्री फसल , अभाव , गरीबी के प्रभावक प्रतीक हैं । वैचारिक चेतना के अभाव मे ठण्ढे हो रहे मनुष्य की नियति है तो सपनों के लिए एकजुटता का आवाहन है और परिवर्तनों के बीच नवनिर्माण का संकल्प है । उनकी कविता नब्ज को पढा जाना चाहिए इस कविता मे मुल्क की बदहाली और तंगहाली का चित्र बडा ही सचेष्ट और वैचारिक है । इस कविता का मुख्य कहन है कि जब देश मे संसाधनों की कमी नही है तो इतनी गरीबी और अभाव क्यों है कहां जाता है इन संसाधनों के दोहन से अर्जित धन ” जहाँ इतने फौलादी हाथ / और आला दिमाग / देश का नक्सा बदलने मे लगे हों / वहाँ / एक गरीबी और पन आसरे का नक्सा नही बदल सकते” जिस देश की श्रमशक्ति फौलादी है । संसाधनों मे कमी न हो और देश का विकास हो रहा हो उस देश मे गरीबी का नक्सा क्यों नही बदल रहा है ।
सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यह आक्रोश धूमिल के आक्रोश जैसा है ।धूमिल भी मोहभंग के कवि थे और पारसनाथ सिंह भी मोहभंग के कवि थे । लेकिन अन्तर यह था कि धूमिल का आक्रोश गुस्से को रूपायित करता है और कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह का आक्रोश बदलाव की शिफारिस करता है । धूमिल सबको तोड कर ध्वन्स कर देना चाहते हैँ उनकी कविता मे भविष्य का वैकल्पिक नक्सा नही है ।पारसनाथ सिंह के पास वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद है । बाकी लोकतन्त्र की आलोचना मे धूमिल जिस तरह लोकजीवन के मुहावरों का प्रयोग करते हैं वही काम पारसनाथ सिंह भी करते हैं इस सन्दर्भ मे उनकी चँवरी कविता देखी जा सकती है ” रामकली , लाली , दीना , और बैजू के छाँह के नीचे जनतन्त्र / किसी बहुत बडे कुकृत्य के मुजरिम सा / सिर नीचा किए बैठा है / और कुछ नही हो रहा है / ठंढे लोहे पर टँगी / काठ की घंटियों के सहारे / आँगन के पार द्वार / कठपुतली उर्वसी का यह नाटक / आखिर कब तक जारी रहेगा”
इस कविता के सन्दर्भ में वरिष्ठ आलोचक कामेश्वर त्रिपाठी लिखते हैं कि यहाँ चँवरी समूचे हिन्दुस्तान का चरित्र बन जाती है” एक ऐसा हिन्दुस्तान जहाँ उजाले की उम्मीद नही है और जहाँ उजाले की उम्मीद नही होती है कविता उम्मीद बनकर आती है । कविता मनुष्य की उम्मीद है वह पारसनाथ सिंह लिखते हैं “कविता / मनुष्य के जिन्दा रहने का / सबसे जिन्दा और सबसे उम्दा प्रमाण है / और जहाँ कहीं भी खडी है / मनुष्य उसकी अन्तिम शर्त है” ।
कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह की लोकचेतना भले ही मोहभंग जनित हो लेकिन वह मोहभंग के दशक का अतिक्रमण करते हैं ।वह दशक और युग की सीमा में बाँधकर रखे जाने वाले लेखकों में नही है ।उनकी कविता का फलक व्यापक है फलतः वह देश की सीमाओं को तोडती है और समस्याएं वैज्ञानिक नजरिए की समझ है इसलिए वह काल की सीमाओं को भी तोडती हैं । हिन्दी कविता की बहुत बडी कमी है कि बडे से बडा कवि भी तात्कालिकता के मोह का परित्याग नही कर पाता है । तात्कालिक कविता कुछ समय तक ताजी रहती है और कुछ समय बाद बासी होने लगती है ।
पारसनाथ की कविता का जब भी पाठ होगा वह युग के साथ युग के अनुरूप समय से टकराती मिलेगीं इन कविताओं का पाठ हर युग मे ताजा रहता है । जैसे आजकल का समय वैश्वीकरण और साम्प्रदायिक फासीवाद का समय है आज पूँजीकृत मुद्दे विस्थापित हो गये ह़ै और उनकी जगह नये नये सवाल और मुल्क की साझा संस्कृति के समक्ष नयी चुनौतियाँ खडी कर दी गयी हैं । कुमारेन्द्र पारस के गीतों में राम और रहीम के बीच विद्यमान पूँजी की करतूतों का जिक्र हुआ है । नब्बे के दशक से लेकर अब तक इतिहास यही कहता है कि साम्प्रदायिक शक्तियाँ इतनी मजबूत कभी नही रही जबसे आर्थिक उदारीकरण बढा है और पूँजी व सत्ता का एकीकरण हुआ है तबसे फासीवाद की नयी आहटे और भी तेजी से सुनाई देने लगी है बात का जिक्र देखिए “राम और राम के बीच गायब राम ही होता है,/ लड़ता रह जाता है नाम उसका। भीतर से ताला / बंद कर लेता है अल्ला और ईसा बाहर सूली / पर चढ़ता है। नदी पर बांध देने वाला घुटने भर / पानी में डूबता है, अपने आप टूटता पहाड़ तोड़ने वाला।“
कुमारेन्द्र की कविता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है लिखा जा सकता है । लेकिन सबसे बडी बात है कि वह प्रतिरोध और संवेदन की आत्मीय व बहुरंगी छटा के साथ भी , लोकतन्त्र और उसकी करतूतों का पर्दाफास करने के बाद भी , शोषक और शोषित के यथार्थ बिम्ब देने के बाद भी अपनी विचारधारा और चेतना से पृथक नही होते हैं तमाम असंगतियों और दुःख द्वन्दों से मुठभेड करते हुए विद्रोह और अतिचार का प्रतिरोध करते हैं ।निराशा और हताशा के स्वरों का सर्वथा अभाव है वह गहन उम्मीद के साथ विचारधारा के साथ शब्दों को सक्रिय करते हैं जैसी सक्रियता उनकी विचारधारा मे है वैसी ही सक्रियता कठिन दौर के कोख मे दबी उम्मीद मे भी है वह अन्धेरे समय में उजली उम्मीदों के कवि हैं “सभी / नीली नींद में डूबे रहते हैं अपनी / मगर तब भी / पर्त-पर-पर्त पड़े अंधेरे की / छाती छेदती रहती है
अपना पूरे वजूद लिए होती है रौशनी / रौशनी अंधेरे का विलोम नहीं होती।“ कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह की कविता और जीवन को देखकर कहा जा सकता है कि उनकी कविता महज रचना नही है न जीवन का निचोड है वह जीवन की अक्षय ऊर्जा का स्रोत भी है । उनकी कविता इतिहास और मनुष्य के बीच द्वन्दात्मक सम्बन्धों की परख रखती है इसलिए वह निराश नही होते है अपनी कविता के माध्यम से घोषित करते हैं कि अन्धेरा रोशनी का विलोम नही है । उजाले की यही उद्दात संकल्पना उन्हे लोक और सर्वहारा के विशाल समूह से जोडती है मुझे आचार्य शुक्ल का वह कथन याद आ रहा है जिसमे उन्होने कहा था कि “कविता मनुष्य के व्यक्तिगत सम्बन्ध के संकुचित मण्डल से उपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि मे ले जाती है” यह कवि उसी सामान्य भावभूमि मे खडा है । इसलिए अन्धेरों के इस भयानक युग मे भी वह आज भी उम्मीदों की उजली मशाल जला रहा है ।